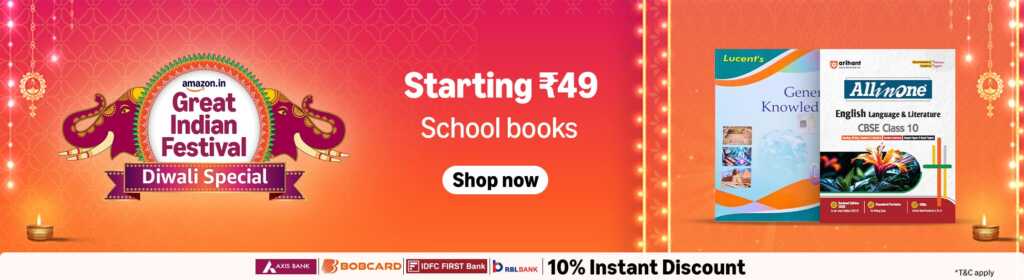others
क्या है वो दलबदल कानून, जिससे नए गुट की मान्यता पा सकते हैं शिवसेना के विद्रोही विधायक
महाराष्ट्र में सियासी स्थिति ने जो घुमाव लिया है, उसमें उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना तो अब करीब तय हो चुका है. शिवसेना के ही एक मंत्री एकनाथ सिंदे ने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर ना केवल पार्टी से विद्रोह कर दिया बल्कि नया गुट बनाने का भी दावा किया. शुरू में उनके साथ 27 विधायक बताए जा रहे थे लेकिन कुछ और विधायकों के उनके साथ मिल जाने से अब वो दावा कर रहे हैं कि अब उनके साथ पार्टी से टूटकर कर 40 विधायक हैं. सबसे पहला सवाल यही है कि क्या दलबदल कानून के तहत वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं या फिर उन्हें नए गुट की मान्यता मिल जाएगी.
फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं. जिसमें शिवसेना के पास 55 विधायक हैं. राष्ट्रवादी क्रांति पार्टी के पास 53 विधायक तो कांग्रेस की ताकत 40 विधायकों की है. इन तीनों पार्टियों ने मिलकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बनाई थी. लेकिन पिछले इस सरकार में शामिल शिवसेना के विधायकों ने बागी तेवर दिखाए तो स्थिति अजीब हो गई.
फिलहाल जो स्थिति है, उसमें अगर कोई सियासी चमत्कार नहीं हो तो उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना करीब तय है.
दरअसल ये कानून तब लागू होता है कि जबकि निर्वाचित सदस्यों द्वारा पार्टी छोड़ने या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है.
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है. इसे 1985 में 52वें संशोधन के साथ संविधान में शामिल किया गया था.
क्यों महसूस हुई इसकी जरूरत
दल बदल कानून की जरूरत तब महसूस हुई जब राजनीतिक लाभ के लिए लगातार सदस्यों को बगैर सोचे समझे दल की अदला बदली करते हुए देखा जाने लगा.अवसरवादिता और राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, साथ ही जनादेश की अनदेखी भी होने लगी. लिहाजा ऐसा कानून बनाया गया कि इस पर रोक लग पाए.
क्या होता है इस कानून से
इस कानून के तहत – कोई सदस्य सदन में पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करे/ यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र दे/ कोई निर्दलीय, चुनाव के बाद किसी दल में चला जाए/ यदि मनोनीत सदस्य कोई दल ज्वाइन कर ले तो उसकी सदस्यता जाएगी.

1985में कानून बनने के बाद भी जब अदला बदली पर बहुत ज्यादा शिकंजा नहीं कस पाया तब इसमें संशोधन किए गए. इसके तहत 2003 में यह तय किया गया कि सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, अगर सामूहिक रूप से भी दल बदला जाता है तो उसे असंवैधानिक करार दिया जाएगा.
इसके अलावा इसी संशोधन में धारा 3 को भी खत्म कर दिया गया जिसके तहत एक तिहाई पार्टी सदस्यों को लेकर दल बदला जा सकता था. अब ऐसा कुछ करने के लिए दो तिहाई सदस्यों की रज़ामंदी की जरूरत होगी.
चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख है
चुनाव आयोग भी इस कानून को लेकर अपनी भूमिका में स्पष्टता चाहता है. इसके अलावा यह मांग भी उठी है कि ऐसे हालात में स्पीकर या अध्यक्ष की राय की समीक्षा भी ठीक से की जानी चाहिए. और तो और स्वेच्छा से दल छोड़ने के अर्थ की भी ठीक से व्याख्या की जाए. क्योंकि इस कानून का इस्तेमाल सदस्य को अपनी बात रखने से रोकने और ‘पार्टी ही सर्वोच्च है’ कि भावना को सही ठहराने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है.
हालांकि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ़ 6 के मुताबिक़ स्पीकर या चेयरपर्सन का दल-बदल को लेकर फ़ैसला आख़िरी होगा. पैराग्राफ़ 7 में कहा गया है कि कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता. लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया लेकिन पैराग्राफ़ 7 को असंवेधानिक क़रार दे दिया.
तब लागू नहीं होगा दल बदल क़ानून
– जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीति पार्टी के साथ मिल जाती है.
– अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं.
– अगर किसी पार्टी के सदस्य दो पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते और विलय के समय अलग ग्रुप में रहना स्वीकार करते है.
– जब किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं.